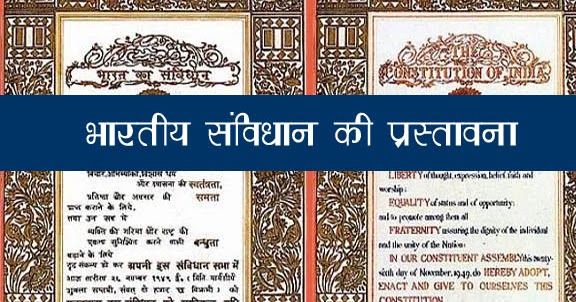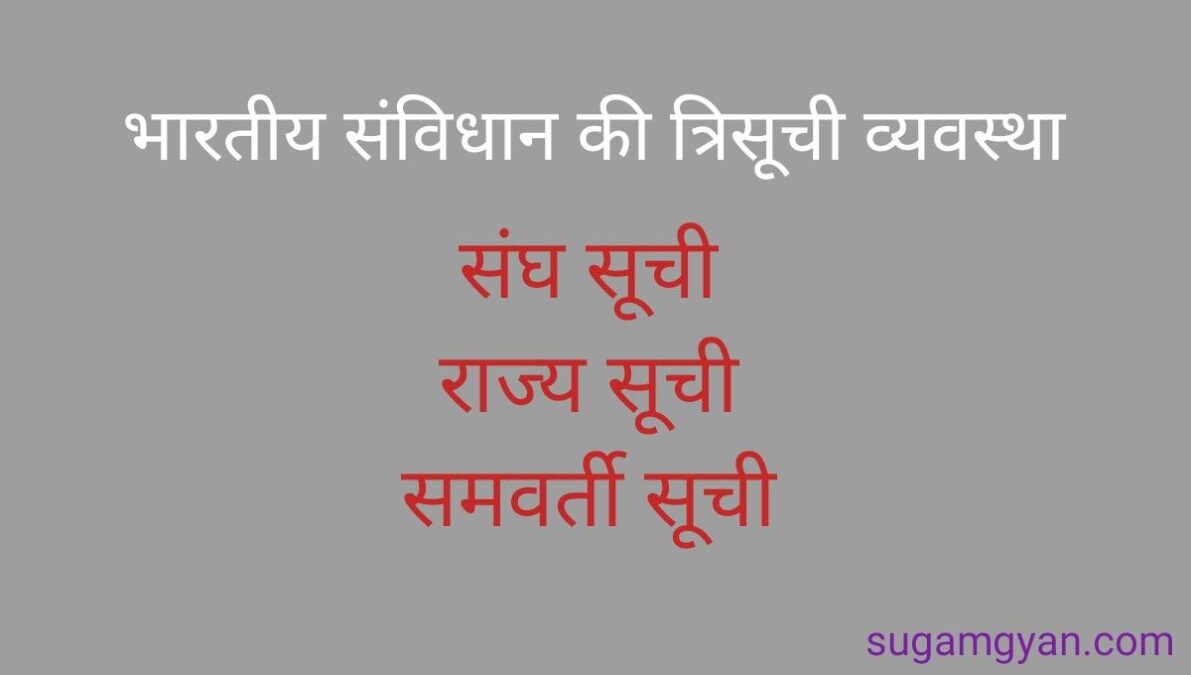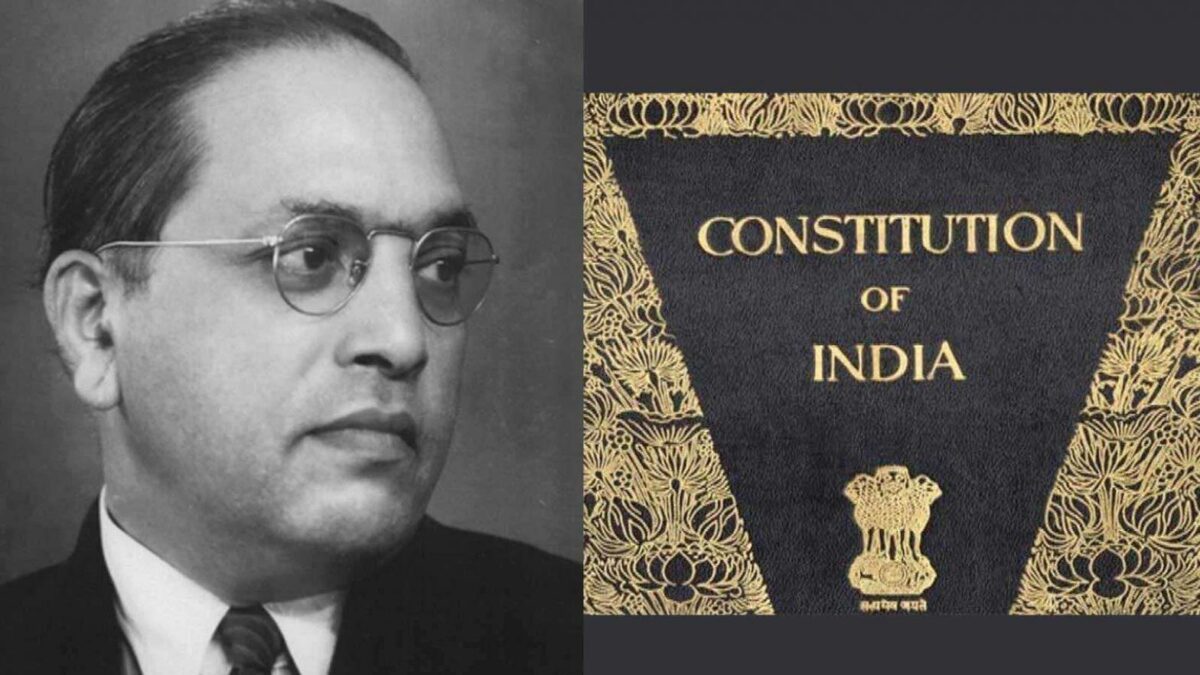भारत का उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) भारतीय न्यायपालिका का शिखर है। इसे देश के संविधान का प्रहरी माना जाता है। इसके गठन का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 124 में वर्णित है। इसी अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गयी। 28 जनवरी 1950 को भारत के उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किया गया। यह देश की सर्वोच्च अपीलीय अदालत है। परन्तु इसके अतिरिक्त दो या अधिक राज्यों के मामले या संविधान में वर्णित मूल अधिकारों के संबंध में वादों को यहाँ सीधे भी रखा जा सकता है।
उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या :-
उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कार्यभार के बढ़ते समय-समय पर बढ़ाई जाती रही है। संविधान के अनुच्छेद 124 (1) के अनुसार न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति संसद के पास है।
26 जनवरी 1950 को स्थापना के समय सर्वोच्च न्यायालय में 1 मुख्य न्यायाधीश (Chief Justice of India) के अतिरिक्त 7 अन्य न्यायाधीश थे। बाद में 1956 में इसे बढाकर 11 (1+10) कर दिया गया। इसके बाद 1960 में इसे 11 से बढ़ाकर 14 (1+13) कर दिया गया। 1977 में इसे फिर बढ़ाकर 18 (1+17) कर दिया गया। 1986 में फिर बदलकर इनकी संख्या को 26 (1+25) कर दिया गया। 2008 में न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ाकर 31 (1+30) कर दिया गया। इस प्रकार मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त अधिकतम 30 अन्य न्यायाधीश भी में हो सकते हैं।
वर्तमान स्थिति –
साल 2019 में कार्यभार को ध्यान में रखते हुए फिर इसमें बदलाव किए गए और न्यायाधीशों की कुल संख्या 34 ( 1 + 33 ) कर दी गई। यही वर्तमान में उच्चतम न्यायालय के कुल न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या है।
वर्तमान मुख्य न्यायाधीश – रंजन गोगोई
रंजन गोगोई ने 3 अक्टूबर 2018 से सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद संभाला। इस पद को ग्रहण करने वाले 46 वें व्यक्ति बने। इस पद पर उनका कार्यकाल 17 नवंबर 2019 तक का होगा। रंजन गोगोई फरवरी 2011 से अप्रैल 2012 तक पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। अप्रैल 2012 में वे सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश नियुक्त किये गए। रंजन गोगोई 1982 में असम के मुख्यमंत्री रहे केशव चंद्र गोगोई के पुत्र हैं।
उच्चतम न्यायालय से सम्बंधित महत्वपूर्ण तथ्य :-
- सर्वोच्च न्यायालय में कार्यरत सभी न्यायाधीशों की निम्नतम आयु सीमा निर्धारित नहीं की गयी है। परन्तु उनके अवकाश ग्रहण करने की अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष है।
- सामान्य तौर पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों में से होती है। परन्तु इसके अतिरिक्त सीधे बार से (वकालत कर रहे वकीलों में से) भी इनकी नियुक्ति की जा सकती है। ऐसा अब तक 8 बार किया भी जा चुका है।
- एम. फातिमा देवी उच्चतम न्यायालय में पहली महिला न्यायाधीश थीं।
- CJI को भारत का राष्ट्रपति शपथ दिलाता है।
- न्यायाधीशों का वेतन भारत की संचित निधि पर भारित है, इसके लिए संसद में मतदान नहीं होता।
- अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय को मूल अधिकारों की रक्षा के लिए रिट जारी करने का अधिकार प्राप्त है।
- अनुच्छेद 124 (2) के तहत उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
- उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को राष्ट्रपति द्वारा साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर संसद की सिफारिश पर समावेदन ( महाभियोग प्रस्ताव ) के आधार पर हटाया जा सकता है। इस प्रक्रिया का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 124 (4) एवं (5) में वर्णित है।
- अनुच्छेद 124 (7) के अनुसार सेवानिवृत्ति के बाद सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते।
- अनुच्छेद 125 (1) के तहत न्यायाधीशों के वेतन का निर्धारण संसद द्वारा बनाई गयी विधि के आधार पर किया जायेगा।
- अनुच्छेद 126 के अनुसार कार्यवाहक CJI की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
- अनुच्छेद 127 (1) में CJI द्वारा उच्चतम न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त करने का प्रबंध किया गया है।
- अनुच्छेद 129 उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय के रूप में घोषित करता है।
- अनुच्छेद 131 में सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार का वर्णन किया गया है।
- अनुच्छेद 132 से 136 तक सुप्रीम कोर्ट के अपीलीय क्षेत्राधिकार का वर्णन है।
- अनुच्छेद 143 के तहत परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार का वर्णन है। इसी अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है।
- तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान सिर्फ उच्चतम न्यायालय हेतु ही है।
- सर्वोच्च न्यायालय की अब तक की सबसे बड़ी खंडपीठ (13 न्यायाधीश) का गठन केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य केस (1973) में किया गया था।
- सर्वोच्च न्यायालय की अब तक की दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ (11 न्यायाधीश) का गठन गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य वाद (1967) में किया गया था।
- संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को है।
भारत के मुख्य न्यायाधीशों की सूची –
| CJI का नाम | कब से | कब तक |
|---|---|---|
| हरिलाल जे. कानिया | 26 जनवरी 1950 | 6 नवंबर 1951 |
| पतंजलि शास्त्री | 7 नवंबर 1951 | 3 जनवरी 1954 |
| मेहरचन्द महाजन | 4 जनवरी 1954 | 22 दिसंबर 1954 |
| बी. के. मुखर्जी | 23 दिसंबर 1954 | 31 जनवरी 1956 |
| एस. आर. दास | 1 फरवरी 1956 | 30 सितंबर 1959 |
| भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा | 1 अक्टूबर 1959 | 31 जनवरी 1964 |
| पी. बी. गजेंद्र गडकर | 1 फरवरी 1964 | 15 मार्च 1966 |
| ए. के. सरकार | 16 मार्च 1966 | 29 जून 1966 |
| के. सुब्बाराव | 30 जून 1966 | 11 अप्रैल 1967 |
| के. एन. वांचू | 12 अप्रैल 1967 | 24 फरवरी 1968 |
| एम. हिदायतुल्ला | 25 फरवरी 1968 | 16 दिसंबर 1970 |
| जे. सी. शाह | 17 दिसंबर 1970 | 21 जनवरी 1971 |
| एस. एम. सीकरी | 22 जनवरी 1971 | 22 अप्रैल 1973 |
| ए. एन. रे | 26 अप्रैल 1973 | 28 जनवरी 1977 |
| एम. एच. बेग | 29 जनवरी 1977 | 21 फरवरी 1978 |
| वाई. वी. चंद्रचूड़ | 22 फरवरी 1978 | 11 जुलाई 1985 |
| प्रफुल्ल नटवरलाल भगवती | 12 जुलाई 1985 | 20 दिसंबर 1986 |
| रघुनंदन स्वरुप पाठक | 21 दिसंबर 1986 | 18 जून 1989 |
| ई. एस. वेंकटरमैया | 19 जून 1989 | 17 दिसंबर 1989 |
| सव्यसाची मुखर्जी | 18 दिसंबर 1989 | 25 सितंबर 1990 |
| रंगनाथ मिश्र | 26 सितंबर 1990 | 24 नवंबर 1901 |
| के.. एन. सिंह | 25 नवंबर 1991 | 12 दिसंबर 1991 |
| एम. एच. कानिया | 13 दिसंबर 1991 | 17 नवंबर 1992 |
| एल. एम. शर्मा | 18 नवंबर 1992 | 11 फरवरी 1993 |
| एम. एन. वेंकटचलैया | 12 फरवरी 1993 | 24 अक्टूबर 1994 |
| ए. एम. अहमदी | 25 अक्टूबर 1994 | 24 मार्च 1997 |
| जे. एस. वर्मा | 25 मार्च 1997 | 17 जनवरी 1998 |
| एम. एम. पुंछी | 18 जनवरी 1998 | 9 अक्टूबर 1998 |
| आदर्श सेन आनंद | 10 अक्टूबर 1998 | 31 अक्टूबर 2001 |
| एस. पी. भरुचा | 1 नवंबर 2001 | 5 मई 2002 |
| बी. एन. किरपाल | 6 मई 2002 | 7 नवंबर 2002 |
| गोपाल बल्लभ पटनायक | 8 नवंबर 2002 | 18 दिसंबर 2002 |
| वी. एन. खरे | 19 दिसंबर 2002 | 1 मई 2004 |
| एस. राजेंद्र बाबू | 2 मई 2004 | 31 मई 2004 |
| रमेश चंद्र लाहोटी | 1 जून 2004 | 31 अक्टूबर 2005 |
| योगेश कुमार सब्बरवाल | 1 नवंबर 2005 | 13 जनवरी 2007 |
| के. जी. बालकृष्णन | 14 जनवरी 2007 | 11 मई 2010 |
| एस. एच. कपाड़िया | 12 मई 2010 | 28 सितंबर 2012 |
| अल्तमस कबीर | 29 सितंबर 2012 | 18 जुलाई 2013 |
| पी. सदाशिवम | 19 जुलाई 2013 | 26 अप्रैल 2013 |
| आर. एम. लोढ़ा | 27 अप्रैल 2014 | 27 सितंबर 2014 |
| एच. एल. दत्तू | 28 सितंबर 2014 | 2 2 दिसंबर 2015 |
| टी. एस. ठाकुर | 3 दिसंबर 2015 | 3 जनवरी 2017 |
| जगदीश सिंह खेहर | 4 जनवरी 2017 | 27 अगस्त 2017 |
| दीपक मिश्रा | 28 अगस्त 2017 | 2 अक्टूबर 2018 |
| रंजन गोगोई | 3 अक्टूबर 2018 से | 17 नवंबर 2019 |
| शरद अरविंद बोबड़े | 18 नवंबर 2019 | 23 अप्रैल 2021 |
| नुथालापति वेंकट रमन | 24 अप्रैल 2021 | 26 अगस्त 2022 |
| उदय उमेश ललित | 27 अगस्त 2022 | 9 नवंबर 2022 |